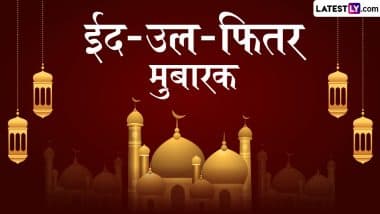नयी दिल्ली, 19 फरवरी उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को इस महत्वपूर्ण कानूनी मुद्दे पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया कि क्या अदालतें मध्यस्थता और सुलह पर 1996 के एक कानून के प्रावधानों के तहत मध्यस्थता निर्णयों को संशोधित कर सकती हैं।
प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति बी आर गवई, न्यायमूर्ति संजय कुमार, न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन एवं न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की संविधान पीठ ने तीन दिनों तक चली सुनवाई में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अरविंद दातार, डेरियस खंबाटा, शेखर नाफडे और रितिन राय सहित वरिष्ठ वकीलों की दलील सुनी।
मेहता ने 13 फरवरी को केंद्र की ओर से अपनी दलील पेश करते हुए पीठ से आग्रह किया था कि देश की बदलती मध्यस्थता आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मध्यस्थता निर्णयों में संशोधन का मुद्दा विधायिका पर छोड़ दिया जाना चाहिए।
हालांकि, दातार ने कहा कि अदालतें, जो कुछ आधार पर मध्यस्थता के निर्णयों को खारिज कर सकती हैं, उन्हें संशोधित भी कर सकती हैं।
नाफडे ने दातार की दलील से सहमति जताते हुए कहा कि अदालतों को मध्यस्थता निर्णयों को संशोधित करने का अधिकार होना चाहिए।
प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने 23 जनवरी को इस विवादास्पद मुद्दे को एक वृहद पीठ के पास भेज दिया था।
मध्यस्थता, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 के तहत विवाद समाधान का एक वैकल्पिक तरीका है और यह न्यायाधिकरणों के निर्णयों में हस्तक्षेप करने में अदालतों की भूमिका को कम करता है।
अधिनियम की धारा 34 प्रक्रियागत अनियमितताओं, सार्वजनिक नीति के उल्लंघन या अधिकार क्षेत्र की कमी जैसे आधार पर मध्यस्थता निर्णय को रद्द करने का प्रावधान करती है।
धारा 37 मध्यस्थता से संबंधित आदेशों के विरुद्ध अपील से संबद्ध है, जिसमें किसी निर्णय को रद्द करने से इनकार करने वाले आदेश भी शामिल हैं।
धारा 34 की तरह, इसका उद्देश्य भी न्यायिक हस्तक्षेप को कम करना है।
(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)













 QuickLY
QuickLY